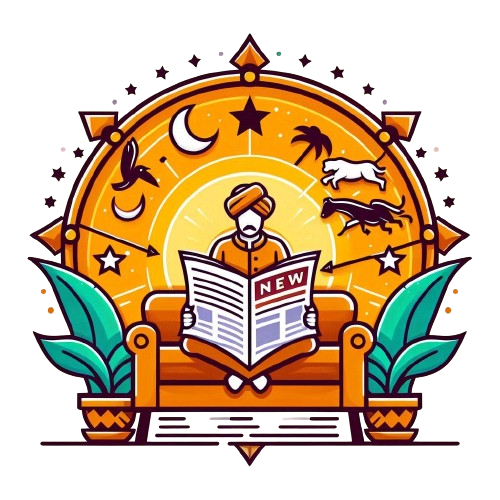जब न्यायाधीश असहमति पर नैतिक पहरेदारी करने लगते हैं और प्रतिशोधात्मक एफआईआर पर चुप रहते हैं, तब न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करना छोड़ देती है और विचारों की निगरानी शुरू कर देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष अली खान महमूदाबाद को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्टों के चलते गिरफ्तारी के बाद अंतरिम जमानत दी है।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया—जो पिछले 36 वर्षों से भाजपा की सदस्य हैं और इस विवाद के बाद सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने की सार्वजनिक इच्छा जता चुकी हैं—ने दावा किया कि महमूदाबाद ने महिला अधिकारियों, विशेष रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का “अपमान” किया है। इन दोनों अधिकारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मीडिया ब्रीफिंग की थी। उनके खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के एक स्थानीय नेता द्वारा दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई।
महमूदाबाद की 8 मई की पोस्ट में कहा गया था कि महिला अधिकारियों को मीडिया ब्रीफिंग में शामिल करना “प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण” है, लेकिन अगर यह ज़मीनी बदलाव के बिना है तो यह “पाखंड” होगा। उन्होंने बुलडोज़िंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए ‘प्रदर्शनात्मक राष्ट्रवाद’ की आलोचना की। इस संतुलित टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर यह बताया गया कि उन्होंने “महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान” किया है और “सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा” दिया है।
हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएँ उन पर लगाईं, जिनमें देशद्रोह जैसे प्रावधान वाला सेक्शन 152 भी शामिल है—जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।
एफआईआर का ढांचा और अदालत की प्रतिक्रिया
इन दोनों एफआईआर की वैधता संदिग्ध है। महमूदाबाद की पोस्ट न केवल विचारशील थी, बल्कि सेना की संयमित कार्रवाई की प्रशंसा करती थी, आम नागरिकों की युद्धोन्मादी सोच की आलोचना करती थी, भारत-पाक रणनीतिक समीकरणों पर विश्लेषण प्रस्तुत करती थी और गीता, पैगंबर मोहम्मद व इमाम अली के हवाले से नैतिक आत्मनिरीक्षण की अपील करती थी। फिर भी इसे राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा गया।
18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिला अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 21 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की। न्यायालय ने महमूदाबाद की भाषा को “डॉग व्हिसलिंग” बताया और पूछा कि वह “सस्ती लोकप्रियता” क्यों चाहते हैं—लेकिन अंततः उन्हें अंतरिम जमानत दी गई। हालांकि, जांच पर रोक नहीं लगाई गई।
पीठ का रवैया और भाषायी नैतिकता
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में सामान्यतः होता है, पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश ही प्रायः फैसला लेते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने एफआईआर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित पूर्ववर्ती फैसलों के आलोक में इसकी समीक्षा की।
इसके बजाय, हरियाणा पुलिस महानिदेशक को एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हरियाणा या दिल्ली से बाहर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हों, ताकि पोस्ट की भाषा और “जटिलता” को समझा जा सके। इसके साथ ही महमूदाबाद का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें भारत-पाक संघर्ष या चल रही केस पर कुछ भी बोलने या लिखने से रोक दिया गया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने समर्थन में खड़े शिक्षाविदों को चेतावनी दी—“हमें उन्हें संभालना आता है”—जो कि सरकारी भाषा की तरह लगता है। अशोका यूनिवर्सिटी के शिक्षक, उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर जेल के बाहर डटे रहे।
न्यायपालिका की चुप्पी और विभाजन
यह भाषा महज़ एक जुबानी फिसलन नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक संदेश है कि यदि राज्य आपके पीछे पड़ जाए, तो अदालत भी शायद आपकी पूरी सुरक्षा नहीं करेगी। जब तक कोई न्यायिक साहस न दिखाए, मौन साधे बैठे जज न्यायिक विश्वासघात के दोषी माने जाएँगे। न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह की चुप्पी इस संदर्भ में पीड़ा देती है।
तुलना और विरोधाभास
कुछ लोग इस केस की तुलना भाजपा मंत्री विजय शाह के केस से कर सकते हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर की गई वास्तविक अपमानजनक टिप्पणी के लिए एसआईटी बनाई थी। लेकिन दोनों मामलों की प्रकृति अलग है—शाह की टिप्पणी सीधी, लिंगभेदी और सांप्रदायिक थी, जबकि महमूदाबाद की पोस्ट एक अकादमिक आलोचना थी।
जमानत—but at what cost?
महमूदाबाद को जमानत तो मिली, लेकिन उस पर भारी शर्तों का पहरा है—पासपोर्ट जब्ती, चुप्पी, और संभावित स्थानीय शर्तें जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तय करेगा। यह सब विचारों की अभिव्यक्ति को एक धीमी, न्यायिक मंजूरी वाली घुटन में बदल देता है।
मुक्त विचारों का दम घोंटना
महमूदाबाद का मामला एक उदाहरण है कि किस तरह बौद्धिक स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है, और समाज को औसत, दोहराव वाली सोच तक सीमित किया जा सकता है। विचारशीलता को “शत्रु” के रूप में देखे जाने वाले राज्य से क्या उम्मीद करें?
न्यायपालिका का विरोधाभासी चेहरा
इसी दिन, सुप्रीम कोर्ट की ही एक अन्य पीठ, न्यायमूर्ति अभय ओका के नेतृत्व में, केरल के पीएफआई केस की सुनवाई में एजेंसी से कहा—“केवल विचारधारा के लिए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता।” इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी केस में भी न्यायमूर्ति ओका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्त पक्ष रखा था।
यह विरोधाभास दर्शाता है कि भारत में फ्री स्पीच का भविष्य किस हद तक “जज के मिजाज” पर निर्भर करता है—एक ही न्यायालय में दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण।
लेखक: सौरव दास 
(सौरव दास एक खोजी पत्रकार हैं, जो कानून, न्यायपालिका, अपराध और नीति पर लिखते हैं।)
![]()